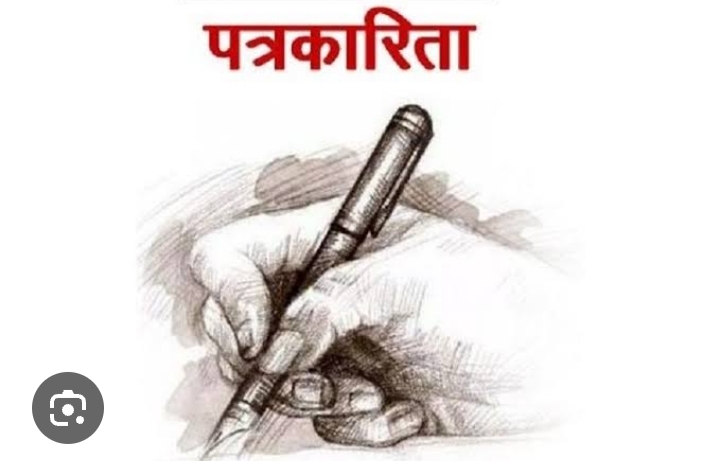सवाल यह है कि पत्रकार की जरूरत जिसको है?
एम हसीन
अभी कल शाम की बात है जब एक अधिकारी ने मुझे आया देखकर अपने चैंबर का दरवाजा बंद करा दिया। शाम को दोबारा गया तो उसने मुझे यह कहकर मिलने से इनकार कर दिया कि “अभी मैं बिजी हूं। कल सुबह मिलने आना।” यह वही अधिकारी है जिसने तीन साल पहले यहां तैनात अपने समकक्ष से जबरदस्ती, ठेकेदारों की फौज के सहारे, चार्ज हासिल करने की कोशिश की थी। कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ पता नहीं। अलबत्ता दो दिन बाद इस अधिकारी को यहां चार्ज मिल गया था। मेरे प्रति इस अधिकारी की असहिष्णुता बेवजह नहीं है। वजह है मेरा पत्रकार होना और अधिकारी की कामयाबी इस बात में है कि जो सवाल मैं उससे पूछने गया हूं उस पर मुझे बैकअप हासिल नहीं है, न पत्रकारों का और न ही जनता का। यह एक बारीक बात है जिसे समझे जाने की जरूरत है। महत्व इस बात की है कि इस भावना के पीछे देश की संवैधानिक नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था है।
मेरी निगाह में बुनियादी सवाल यह है कि पत्रकारिता की जरूरत जिसको है? पत्रकारिता की सामाजिक या संवैधानिक हैसियत क्या है? जहां तक सवाल संवैधानिक हैसियत का है तो वह कुछ नहीं है। कहा जाता है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि ऐसा कैसे है? कारण, जैसे संविधान विधायिका को, न्यायपालिका को और कार्यपालिका को बैकअप देता है, उन्हें निर्णायक शक्ति देता है, ऐसे ही पत्रकारिता को नहीं देता। पत्रकार के कुछ कहे-लिखे या प्रकाशित-प्रसारित किए गए का कोई संवैधानिक या कानूनी महत्व नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स को विधायिका या न्यायपालिका में एविडेंस के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर कार्यपालिका में तो मीडिया रिपोर्ट्स की मान्यता हो ही नहीं सकती क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स तो मुख्यत: कार्यपालिका के विषय में ही होती हैं। संविधान निर्माताओं की सोच इस व्यवस्था के पीछे क्या थी, यह अलग से बहस का विषय है। अहमियत इस बात की है कि ऐसी व्यवस्था में पत्रकारिता की जरूरत किसको है। क्या समाज को? दरअसल, इसे संवैधानिक मान्यताओं के संदर्भ में देखा जाना इतना जरूरी नहीं है जितना सामाजिक मान्यताओं के संदर्भ में देखा जाना जरूरी है।
सवाल यह है कि क्या है हमारी सामाजिक मान्यता या कहें कि व्यवस्था? यह कि जब कोई व्यक्ति कहीं किसी के पास जाता है तो कुछ लेकर जाता है। किसान जब किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या किसी नेता के पास जाता है तो सब्जी लेकर जाता है। पशु पालक दूध, मठ्ठा, घी लेकर जाता है। ग्रामीण क्षेत्र का उत्पादक गुड, शक्कर या ऐसा ही कुछ और लेकर जाता है। बाग का मालिक फल लेकर जाता है। माली फूल या गुलदस्ता लेकर जाता है। यह भारत की प्राचीन व्यवस्था है, जिसमें समय के साथ बदलाव हुआ है। मसलन, शहरी क्षेत्र का व्यक्ति जो, औद्योगिक उत्पादन करता है और किसी के लिए तोहफे के तौर पर दूध, घी, मठ्ठा, शक्कर, फल, सब्जी लेकर भी नहीं जा सकता और अपना उत्पादन भी लेकर नहीं जा सकता वह फूल तो लेकर जा ही सकता है, मिठाई तो लेकर जा ही सकता है, सूखे मेवे के डिब्बे तो लेकर जा ही सकता है। ये सारी चीजें तो बाजार में बिकती हैं और इन्हें कोई भी खरीद सकता है। यह व्यवहार सरकारी दफ्तरों में आम देखने में आता है। अहमियत इस बात की है कि इस सामाजिक मान्यता से “लालच” का नहीं बल्कि “सम्मान” का भाव जुड़ा हुआ है, रुतबे का भाव जुड़ा हुआ है, हुक़्मरानी का भाव जुड़ा हुआ है, “योर लार्ड शिप” का भाव जुड़ा हुआ है। जैसे मंदिर में भगवान पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है वैसे ही अधिकारी को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यही वह परंपरा है जो सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के भीतर दंभ पैदा करती है और उसे व्यक्ति से कहीं ऊपर की चीज बनाती है, उसे जनता के “माइबाप” का दर्जा देती है, बल्कि “भगवान” का दर्जा देती है।
इसी सामाजिक व्यवस्था से दरअसल वह संवैधानिक व्यवस्था आकार लेती है जिसमें पत्रकारिता के लिए कहीं स्थान बाकी नहीं बचता। कारण यह है कि पत्रकार ऐसा प्राणी है जो जब कहीं जाता है तो कुछ लेकर नहीं जाता, कोई गुलदस्ता, कोई उपहार लेकर अधिकारी से मिलने नहीं जाता। पत्रकार अगर पत्रकार है तो वह किसी के पास कुछ लेकर जाता है तो वह होता है “सवाल।” पत्रकार अगर पत्रकार नहीं है तो भी वह अधिकारी के पास कुछ लेकर नहीं जाता, बल्कि कुछ मांगने ही जाता है। दोनों सूरतों में अधिकारी को “पत्रकार” कब मंजूर होता है, कब “कुबूल” होता है?
बुनियादी दिक्कत यह है कि पत्रकारिता को अपने कर्म के लिए वह व्यक्ति चुनता है जो अपनी सोच-समझ के तौर पर या तो सामाजिक व्यवस्था का विरोधी है या फिर संवैधानिक व्यवस्था का पक्षधर है। इस मामले में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि संविधान कोई भी हो, वह अच्छा ही होता है और व्यापक हित में सोचने वाला व्यक्ति संविधान के किन्हीं प्रावधानों से सहमत न होते हुए भी संविधान का विरोधी नहीं होता, वह संविधान का विरोध नहीं करता; यहां तक कि वह धार्मिक संविधानों का विरोध भी नहीं करता। इसे यूं समझा जाए कि जो व्यक्ति आस्तिक न हो, भगवान में विश्वास न करता हो वह भी धार्मिक संविधानों का पूरे तौर पर विरोध नहीं करता, धार्मिक संविधानों का वह बुनियादी विरोधी नहीं होता बल्कि वह धार्मिक व्यवस्था के नाम पर थोपी जाने वाली व्यवस्था का विरोधी होता है। सारी दुनिया में कम्युनिस्ट भले ही धार्मिक न माने जाते हों, लेकिन किन्हीं धार्मिक प्रावधानों का पालन करते हुए कम्युनिस्टों को भी देखा जा सकता है।
अब मसला यह है कि कुछ लेकर आने वाले का स्वागत तो हर जगह होना ही हुआ होता है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में इसी व्यवस्था के तहत कुछ लेकर आने वाले का स्वागत होता है। लेकिन जन-भावना के चलते यूं खुद को “माई बाप” बल्कि “भगवान” समझ लेने वाले अधिकारी क्या वाकई “भगवान” बन जाते हैं? वे जो करोड़ों के घपले करते हैं, उसी जनता के अधिकारों पर डाका डालते हैं जो उन्हें “भगवान” बनाती है, वे क्या “भगवान” बनाए जाने लायक हैं? जब कोई पत्रकार इसी सवाल को उठाता है तो जनता पत्रकार के साथ नहीं बल्कि अधिकारी यानी “अपने भगवान” के साथ खड़ी नजर आती है। तो क्यों न समझा जाए कि पत्रकार की जरूरत किसी को नहीं है।